Description
महादेवी वर्मा आधुनिक युग की प्रमुख कवयित्री के रूप में अधिक ख्यात हैं। परन्तु जब साहित्य-अध्येता उनके गद्य-साहित्य से थोड़ा भी परिचय प्राप्त करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कवयित्री का गद्य कार रूप कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका जन्म फाल्गुन पूर्णिमा (वसन्तोसव) के दिन 1907 ई. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। सन 1912 ई. में इन्दौर के मिशन स्कूल में उन्हें भरती कर दिया गया। घर में हिन्दी, उर्दू, चित्रकला और संगीत की पढ़ाई के लिए एक पंडित, एक मौलवी, एक चित्र-शिक्षक तथा संगीत-शिक्षक का प्रबन्ध कर दिया गया। गंगा प्रसाद पांडेय ने अपनी पुस्तक “महीयसी महादेवी” में उनके बालपन का जिक्र करते हुए लिखा है, “पढ़ाई प्रारम्भ के प्रथम दिन ही आप थोड़ी देर तक अध्यापक के पास बैठी रहीं और फिर छुट्टी की मांग पेश की। आवश्यकता पूछने पर उत्तर मिला-फूल तोड़ लाऊँ नहीं तो माली तोड़कर बाबू (पिता जी) के गुलदस्ते में लगा देगा, जहाँ वे सूख जाते हैं। “तो कया तुम्हारे तोड़ने से नहीं सूखते ?” सूखते तो हैं, पर भगवान जी पर चढ़ने के बाद। अब तक महादेवी ने अपनी करुण कोमल कविता से ही साहित्य में प्रवेश किया था। “अतीत के चल-चित्र” उनकी प्रथम गद्य-पुस्तक है। रचना चाहे गद्य की हो, चाहे पद्य की, उसमें साहित्यकार के व्यक्तित्व का भाव अवश्य रहता है। साहित्यकार जो कुछ लिखता है, उस पर उसके अनुभवों, विचारों तथा मनोभावों की छाप उसी प्रकार रहती है, जिस प्रकार वस्तु की स्थिति के साथ उसकी छाया। यह छाया कभी स्पष्ट और कभी अस्पष्ट होती है, किन्तु उसका अस्तित्व अमिट रहता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्त्रियों की दीन-दशा पर महादेवी वर्मा ने जो कार्य किया आज के इस युग में उसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन कार्य होगा। स्त्री विषयक चिंतन पर महादेवी जी ने अपना सारा जीवन गुजार दिया, वह मरते दम तक स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती रहीं। वह खुद स्त्री होने के नाते स्त्री की पीड़ा को भली-भांति जानती थी और समझती थी। ‘‘नारी में परिस्थितियों के अनुसार अपने बाह्य जीवन को ढाल लेने की जितनी सहज प्रवृति है, अपने स्वभावगत गुण न छोड़ने की आन्तरिक प्रेरणा उससे कम नहीं-इसी से भारतीय नारी भारतीय पुरुष से अधिक सतर्कता के साथ अपनी विशेषताओं की रक्षा कर सकी है, पुरुष के समान अपनी व्यथा भूलने के लिए वह कादम्बिनी नहीं माँगती, उल्लास के स्पन्दन के लिए लालसा का ताण्डव नहीं चाहती क्योंकि दुःख को वह जीवन की शक्ति-परीक्षा के रुप में ग्रहण कर सकती है और सुख को कर्तव्य में प्राप्त कर लेने की क्षमता रखती है।’’
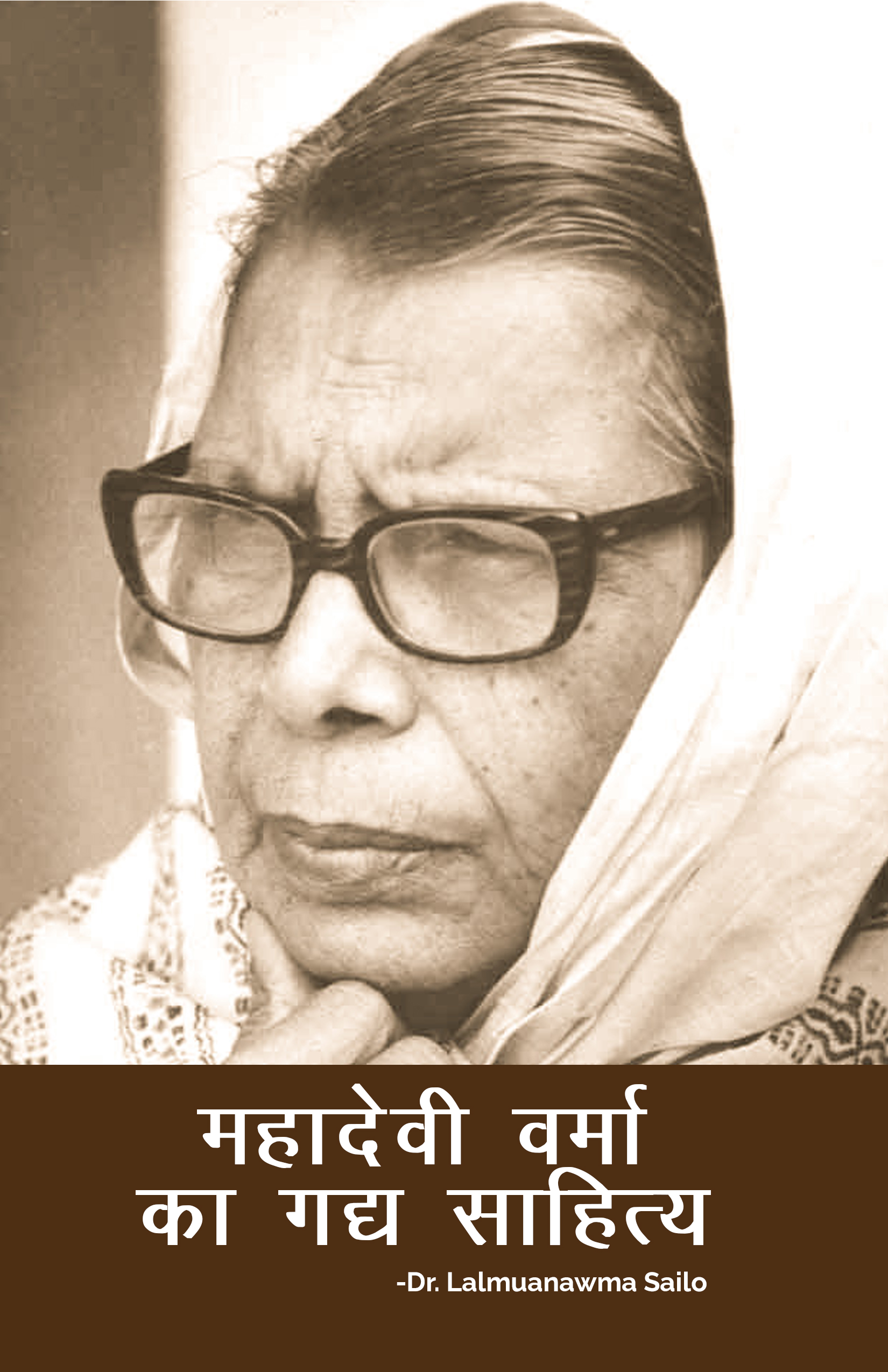
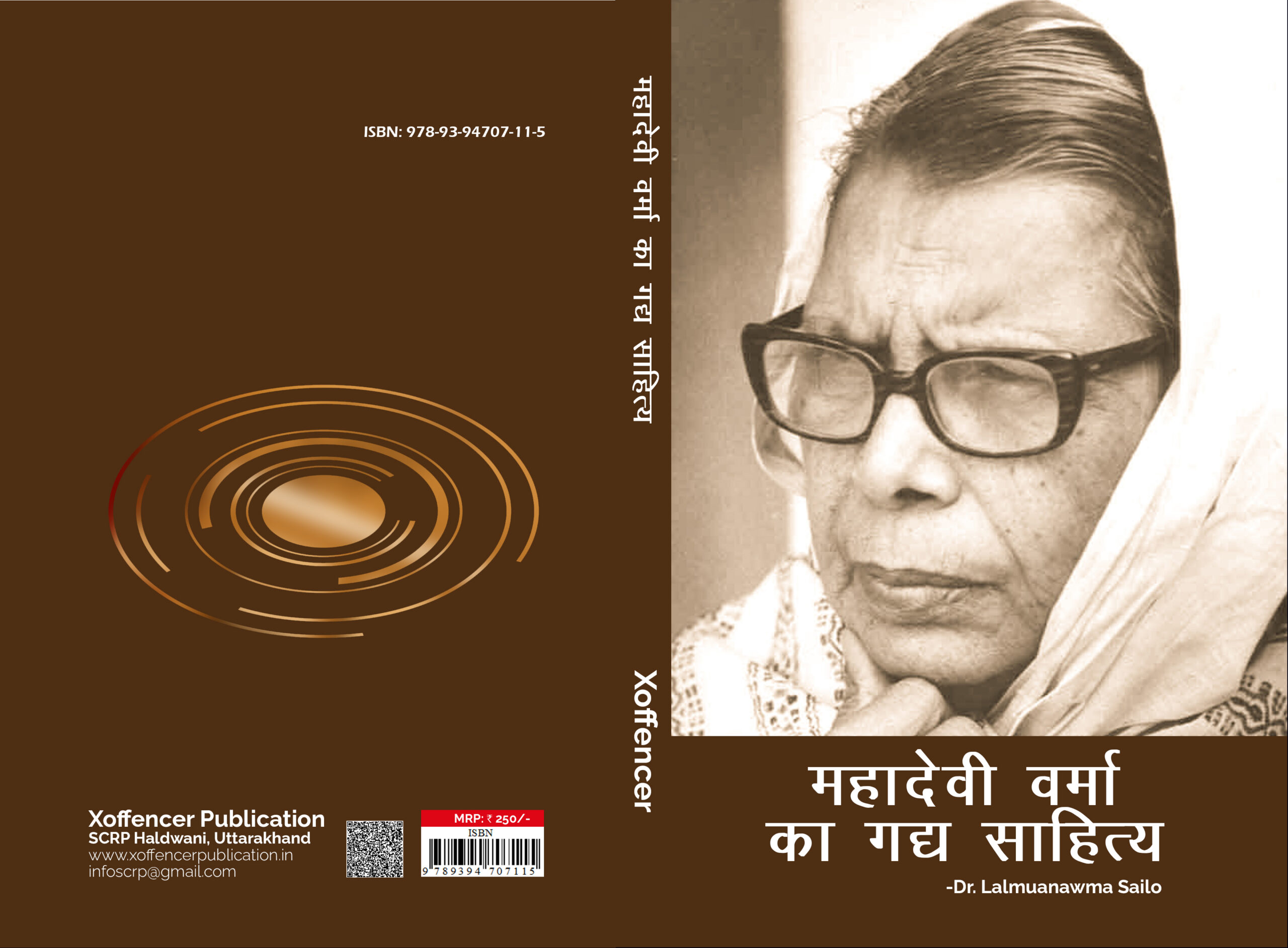
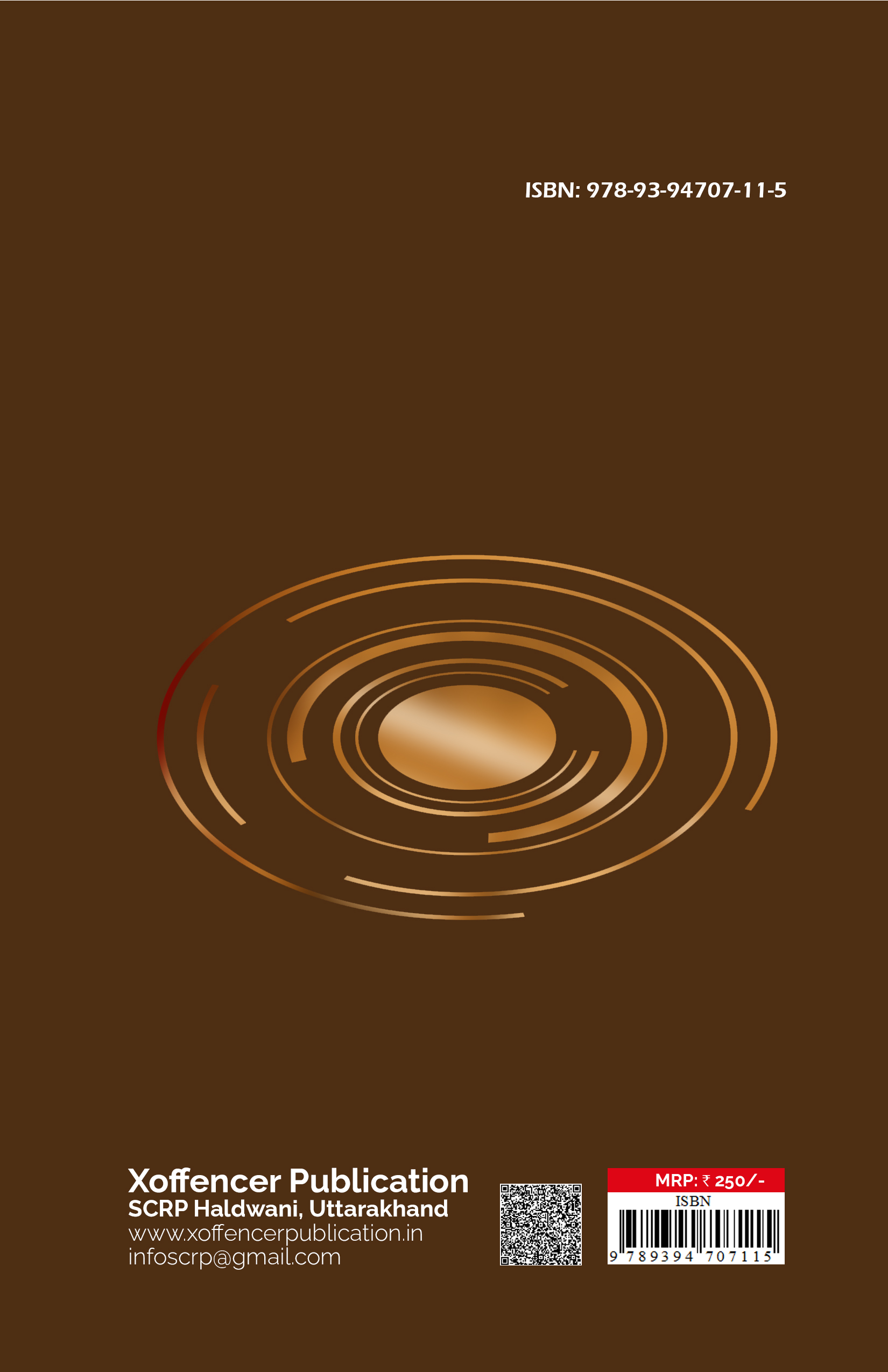

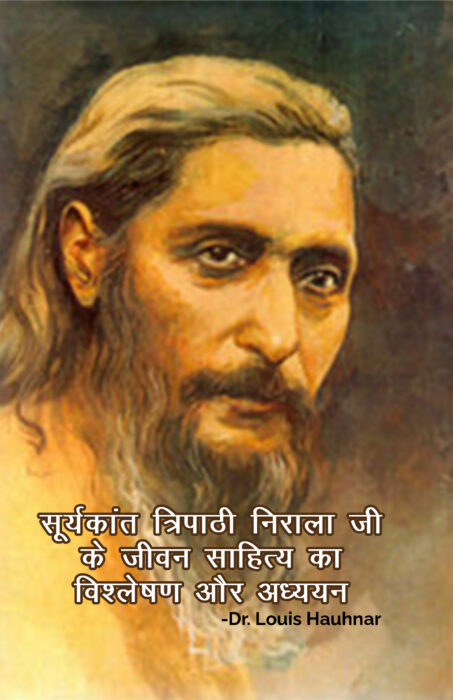
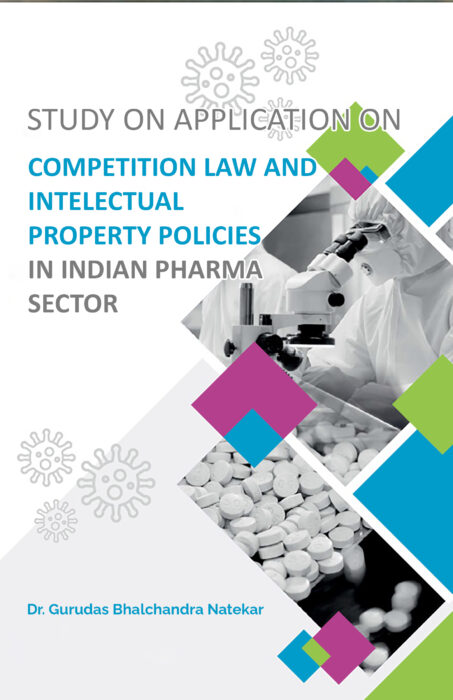
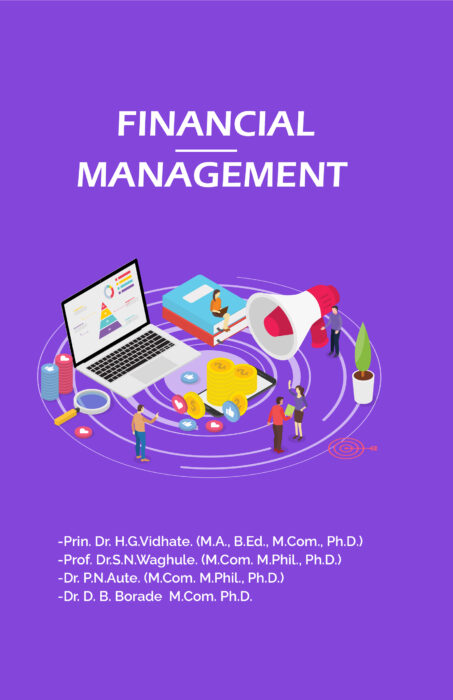
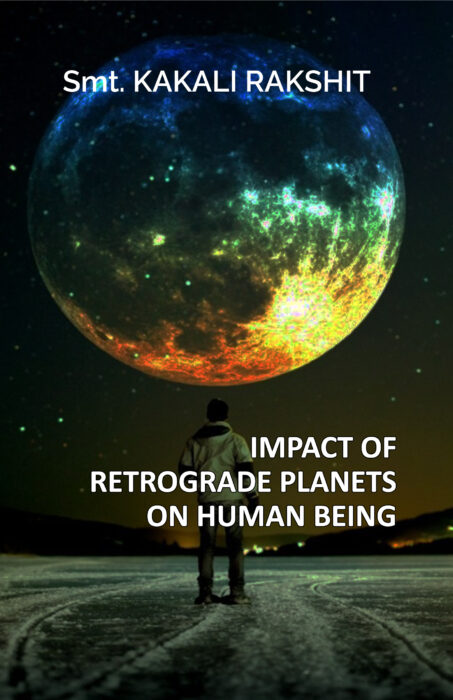
Reviews
There are no reviews yet.